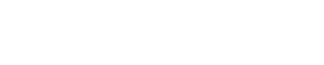
बड़ी खबरें
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता की आस्था और भरोसे की कसौटी भी होते हैं। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता ही इस भरोसे की नींव है। लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग की एक पहल ने देश की राजनीति और समाज दोनों को गहरे सवालों में डाल दिया है।
SIR: लोकतंत्र की मजबूती या सत्ता का नया हथियार?
यह पहल है विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR)। चुनाव आयोग का दावा है कि इससे मतदाता सूची को पूरी तरह साफ और निष्पक्ष बनाया जाएगा, ताकि 2026 तक किसी भी चुनाव में पारदर्शिता पर उंगली न उठे। लेकिन विपक्षी दलों और कई नागरिक संगठनों का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता से ज्यादा "राजनीतिक हस्तक्षेप" का रास्ता खोल देगा। तो सवाल है – क्या यह कदम लोकतंत्र की मजबूती के लिए है या फिर सत्ता की राजनीति का एक नया हथियार? आइए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं।
क्या है SIR?
भारत में चुनाव से पहले मतदाता सूची का लगातार अपडेट होना जरूरी है। इसमें मुख्य काम होता है:
मृत लोगों के नाम हटाना,
18 साल के नए मतदाताओं को जोड़ना,
जिन लोगों ने जगह बदली है उनके पते बदलना,
और गलत प्रविष्टियों को सुधारना।
SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस प्रक्रिया का एक बड़ा और गहन संस्करण है। इसमें सिर्फ कागज पर सुधार नहीं, बल्कि घर-घर जाकर जांच, बूथ स्तर पर सत्यापन, डिजिटल प्रमाणीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी शामिल होगी। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि 2026 तक एक ऐसी मतदाता सूची तैयार की जाए जो पूरी तरह साफ, अद्यतन और विवाद-मुक्त हो।
विवाद क्यों खड़ा हुआ?
कागज पर देखें तो SIR सुनने में बिल्कुल सही और लोकतंत्र के लिए उपयोगी लगता है। लेकिन जब बात राजनीति की हो, तो कोई भी प्रक्रिया विवाद से बच नहीं पाती। SIR पर उठाए जा रहे बड़े सवाल ये हैं:
1. राजनीतिक हस्तक्षेप का डर
विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार मतदाता सूचियों में चयनात्मक बदलाव करा सकती है। यानी कुछ खास इलाकों या समुदायों के नाम हटाए या जोड़े जा सकते हैं, जिससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा। यह आरोप इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भारत जैसे विविधता वाले देश में मतदाता प्रोफाइल बदलना सीधे राजनीति की दिशा बदल सकता है।
2. तकनीकी अपारदर्शिता
SIR में आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र (EPIC) को लिंक करने की बात है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डेटा प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी चिंता यह है कि गरीब, ग्रामीण और तकनीकी रूप से कमजोर समुदाय डिजिटल प्रक्रिया से पीछे छूट जाएंगे। इससे लोकतंत्र में उनकी भागीदारी कम हो सकती है।
3. संस्थागत विश्वास पर सवाल
चुनाव आयोग अब तक भारत की लोकतांत्रिक विश्वसनीयता की रीढ़ माना जाता रहा है। लेकिन जब उस पर बार-बार राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगते हैं, तो जनता का भरोसा कमजोर होता है। यही भरोसा लोकतंत्र की असली ताकत है।
4. नागरिक सहभागिता की कमी
भारत के दूरदराज इलाकों, आदिवासी समुदायों, प्रवासी मजदूरों और गरीब तबके तक SIR की जानकारी और प्रक्रिया पहुँचाना बड़ी चुनौती है। अगर ये लोग सूची से बाहर रह गए तो यह लोकतंत्र की सबसे कमजोर कड़ी बन जाएगी।
संविधान और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं?
भारत का संविधान चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र अधिकार देता है कि वह चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए।
सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार आयोग की स्वतंत्रता पर जोर दे चुका है:
केशवानंद भारती केस (1973): लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।
टी.एन. शेषन केस (1995): चुनाव आयोग को निष्पक्षता का संरक्षक बताया गया।
पीयूसीएल केस (2003): मतदाता का स्वतंत्र अधिकार और पारदर्शिता चुनावी सुधारों की आत्मा है।
इसका मतलब है कि मतदाता सूची केवल तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का प्रश्न है।
क्या असर पड़ेगा इस विवाद का?
जनता के भरोसे पर असर:
अगर मतदाता सूची पर भरोसा नहीं रहा, तो जनता का लोकतंत्र से मोहभंग हो सकता है।
राजनीतिक ध्रुवीकरण:
हर बार सूची पर विवाद होगा तो दल आपस में सहमति बनाने के बजाय और बंटेंगे।
संस्थागत संकट:
अगर आयोग को केवल “सरकारी एजेंसी” समझा जाने लगा, तो उसकी साख कमजोर होगी।
अंतरराष्ट्रीय छवि:
भारत अब तक चुनावी पारदर्शिता का मॉडल माना जाता रहा है। विवाद बढ़ने से यह छवि भी धुंधली हो सकती है।
क्या हो सकती है सुधार की दिशा?
इस विवाद को खत्म करने और मतदाता सूची को सचमुच पारदर्शी बनाने के लिए कुछ कदम जरूरी हैं:
प्रौद्योगिकी का संतुलन: आधार-EPIC लिंकिंग को पूरी तरह स्वैच्छिक बनाया जाए और डेटा प्राइवेसी कानूनों का पालन किया जाए।
स्वतंत्र निगरानी: चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं का ऑडिट किसी स्वतंत्र समिति द्वारा किया जाए जिसमें न्यायपालिका और नागरिक समाज भी शामिल हों।
जन-जागरूकता: ग्रामीण इलाकों, महिलाओं, आदिवासियों और प्रवासियों तक विशेष अभियान चलाकर पहुँच बनाई जाए।
संवैधानिक सुधार: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाए। इसके लिए कोलेजियम जैसी व्यवस्था हो सकती है।
दूसरे देशों से क्या सीख सकते हैं?
यूके: हर साल घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन।
अमेरिका: कई राज्यों में स्वचालित मतदाता पंजीकरण।
ऑस्ट्रेलिया: अनिवार्य मतदान और मजबूत स्वतंत्र चुनाव आयोग।
जनता का भरोसा ही लोकतंत्र की असली नींव
भारत इन मॉडलों से प्रेरणा लेकर अपनी प्रक्रिया को और पारदर्शी और सहभागी बना सकता है।लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं चलता, बल्कि उस पर जनता के भरोसे से चलता है। SIR जैसी पहलें तभी सफल होंगी जब वे पूरी तरह पारदर्शी और सहभागी हों। आज चुनौती यह नहीं है कि मतदाता सूची कितनी "साफ" है, बल्कि यह है कि जनता उसे कितना निष्पक्ष मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है – “मुक्त और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की जीवनरेखा हैं।” अगर मतदाता सूची या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर संदेह बना रहा, तो यह लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर कर सकता है। SIR विवाद यही याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताकत उनके आदेशों से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से आती है।
By Ashutosh Mishra
(लेखक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के विशेष जानकार हैं।)

Baten UP Ki Desk
Published : 20 August, 2025, 8:06 pm
Author Info : Baten UP Ki